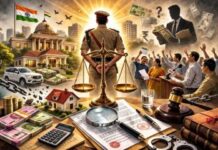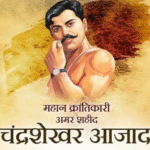गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने कहा था, ‘आम लोग जज को न्याय देने वाले भगवान की तरह देखते हैं लेकिन फिर भी कोर्ट-कचहरी के नाम से डरते हैं। वहां जाने से बचने के लिए वे अपने जीवन में कई तरह के अन्याय चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं।’ स्पष्ट है कि इसका कारण दशकों जारी रहने वाली अंतहीन खर्चीली प्रक्रिया है जो न्याय की आशा लेकर न्याय की चैखट पर पहुंचे व्यक्ति का मनोबल तोड़ देती है। हाँ, जो लोग हर पेशी पर लाखों लेने वाले वकीलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सामथ्र्य रखते हैं उन्हें जरूर राहत मिलती है। आज अच्छे वकील की परिभाषा उसके कानूनी ज्ञान अथवा अनुभव से अधिक व्यवस्था से न्यायाधिकारी तक सेटिंग की उसकी क्षमता की ओर मुड़ चुकी है। पिछले दशक में सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता का वह वायरल अश्लील विडियो किसे याद न होगा जिसमें वह यौन शोषण करते हुए जज बनाने का आश्वासन दे रहा था तो वर्तमान में एक जज के घर लगी आग के बाद करोड़ो की नकदी जलने के समाचार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो हम न्यायिक अराजकता के दौर में जी रहे हैं जहां जज की नियुक्ति जज करेंगे, जज की गलती की जांच भी जज करेंगे और फैसला भी जज ही करेंगे। न्याय की कसौटी पर वर्तमान न्यायिक परिस्थितियां
पीढ़ी दर पीढ़ी न्यायपालिका के सिरमौर बनने-बनाने अर्थात बने रहने का खेल चल रहा है परंतु देश की संसद द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को व्यवस्थित करने के लिए विधिवत पारित कानून को खुद न्यायालय ही रद्द कर देती है। दुनिया भर की गलतियों पर कड़ी टिप्पणी करने वाली न्यायपालिका अपने अंदर झांकने का नैतिक साहस नहीं जुटा रही तो देश के उस सामान्य व्यक्ति के लिए न्याय का क्या अर्थ रह जाएगा जो माननीया राष्ट्रपति जी के कथनानुसार, ‘जज को न्याय देने वाले भगवान की तरह देखते हैं।’
यह निर्विवाद सत्य है कि कोई भी मनुष्य गलतियों से परे नहीं हो सकता, इसीलिए तो न्यायिक समीक्षा में जिला न्यायालय का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द करने अर्थात् पलटने के एक नहीं, हजारों-लाखों उदाहरण है। तो नियुक्ति के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) की तरह बजाय कॉलेजियम का क्या औचित्य है। जो कॉलेजियम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम का चयन कर सरकार के पास भेजता है और कॉलेजियम की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी है, उसमें शामिल लोग कोई गलती, भेदभाव, पक्षपात कर ही नहीं सकते , ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इस सत्य को देश के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथियों को स्वीकार कर नई और अधिकतम निर्दोष व्यवस्था बनाने के लिए पहल क्यों नहीं करनी चाहिए…?
यदि साधारण मामलों का स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाई करने वाली न्यायपालिका न्याय व्यवस्था के इन दोषों को स्वीकार नहीं करती तो देश की जनता द्वारा चुनी हुई संसद को देश के सामान्य व्यक्ति के विश्वास की रक्षा के लिए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, प्रत्येक जज के लिए हर वर्ष अपनी और अपने परिवार की आय और जल-अचल की घोषणा अनिवार्य बनानी चाहिए। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यायिक सुधार के लिए बनाए जाने वाले काननू को संविधान की नौवी अनुसूची में शामिल करना चाहिए ताकि उसे रद्द करने की आशंका ही न रहे। ज्ञातव्य है, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़े गई इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी भी संस्थान को अपने हित में मनमानी की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?
यह सर्वज्ञात है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की सबसे बड़ी अदालत के कुछ फैसलों पर तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई। पूर्व में अदालत के निर्णय पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया का प्रचलन नहीं था, इसलिए इसे एक नई परम्परा कहा जा सकता है लेकिन प्रश्न है कि क्या अदालत के किसी निर्णय पर ईश्वरीय आदेश की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए? इसका उत्तर शायद देश की सबसे बड़ी अदालत भी ‘हां’ में नहीं देगी क्योंकि जिला अदालत के निर्णय को गलत बताते हुए उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील का संवैधानिक प्रावधान है। अनेक बार उच्चतम न्यायालय की बैंच के सदस्यों को भी परस्पर विरोधी निष्कर्ष प्रस्तुत करते देखा गया है. अतः कहा जा सकता है कि ‘किसी भी फैसले में ऐसे ऐसी बातें होना संभव है जिससे असहमति हो सकती है।’ बेशक कोर्ट के फैसले से मतभिन्नता अथवा नाराजगी का प्रदर्शन भारत के लिए यह नई परम्परा है लेकिन विश्व के अनेक देशों में अदालत के फैसले से असहमति व आलोचना का प्रचलन है। न्याय की कसौटी पर वर्तमान न्यायिक परिस्थितियां
कुछ वष्र पूर्व रोहिंग्या शरणाथियों को शरण देने के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानवीय आधार पर गैर कानूनी रूप से भारत में घुसे लोगों का पक्ष लेना देश की सुरक्षा के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि इन रोहिंग्या शरणाथियों को भारत में रहने की अनुमति देने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि सुरक्षा संबंधी कोई चूक या दुर्घटना होती है तो कार्यपालिका को जिम्मेवार ठहराया जाता है तो उसकी राय की अनदेखी करते हुए मामले को लटकाने पर प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। यहां विशेष रूप से स्मरणीय है कि उच्चतम न्यायालय को जिस संविधान का संरक्षक कहा जाता है, उसी संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के कर्तव्यों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। इस बात पर स्वयं सरकार को अदालत को विचार करना चाहिए कि क्या रोहिंग्या मामले में माननीय अदालत का आदेश इस प्रावधान की मूल भावना के साथ कितना न्याय करता है।
आज सामान्यजन के मन में भी यह प्रश्न उठ रहा है कि माननीय न्यायालय को गलियों, सड़कों, नालियों की गंदगी, प्रदूषण तो दिखाई देता है लेकिन क्या कारण है कि देश की अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, विलम्ब दिखाई नहीं देता? दशकों से लम्बित मामलों के निपटान पर सवाल उठने पर कहा जाता है कि ‘न्यायाधीशों की कमी है’। निश्चित रूप से यह तर्क सही है लेकिन व्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में भी स्टाफ की समस्या है। उन्हें तो इस कमी के लिए न्यायालय ने कभी दोष मुक्त नहीं किया।
न्याय में देरी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका पूरा जीवन ही न्याय के इंतजार में बीत गया। कहा गया है ‘जस्टिस डिलेड इज, जस्टिस डिनाइड’ अर्थात् ‘न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना ही है’ परंतु फैसले के बाद भी फैसले की प्रति प्राप्त करना आसान नहीं है। किसी दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र नहीं, देश की राजधानी की द्वारका अदालत ने फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में निर्णय घोषित किया। तत्काल सशुल्क आवेदन करने के बावजूद दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई। जब भी इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, ‘आपको शीघ्र एसएमएस प्राप्त हो जाएगा।’ जैसा रटा-रटाया उत्तर प्राप्त होता है परंतु स्टाफ सूत्रों के अनुसार निर्णय देने वाले जज साहब विस्तृत निर्णय लिखने के लिए संबंधित फाइल अपने साथ अपने ले गए हैं। इसी बीच उनका दो बार ट्रांसफर हो चुका है। न्याय की इस गति के कारण बेशक व्यंग्य के कारण ही सही, ‘अच्छे वकील’ की बजाय ‘जज’ से सम्पर्क की बाते कही जा रही है।
न्याय प्रदान करने के मूल कार्य को प्राथमिकता देने की बजाय लंबी तारीखे देती है जबकि अन्य मामलों को तत्काल सुना जाना दशकों से अदालतों में न्याय की आशा में धक्के खा रहे निर्दोष लोगो के साथ न्याय कैसे है? न्याय का सर्वभौमिक सिद्धांत है, ‘बेशक हजार दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या न्याय की आशा में दशकों अदालतों में चक्कर काटने वाले ‘निर्दोषों’ पर न्याय का यह सर्वभौमिक सिद्धांत लागू नहीं होता…? महामहिम राष्ट्रपति जी ने गत वर्ष जो कहा था, वह नई घटनाओं के कारण आज अधिक प्रासंगिक है इसलिए न्याय की गरिमा को अक्षुण रखने के लिए बिना देरी, तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। न्यायालय को अच्छे निर्णय के लिए प्रशंसा मिलती है तो उसके साये तले पनपे गलत कामों पर सवाल उठाने का उद्देश्य न्यायालय की अवमानना अथवा उसका निरादर नहीं है। न्याय की कसौटी पर वर्तमान न्यायिक परिस्थितियां