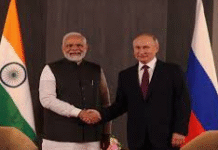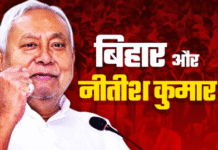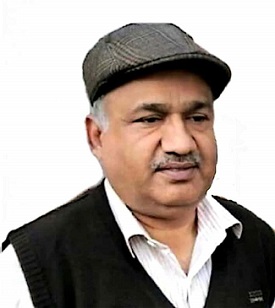
मनरेगा वित्तीय मामले में देश की अन्य सभी योजनाओं से बिल्कुल अलग मानी जाती रही है। इस योजना को प्रारंभ में नरेगा नाम से चलाया गया था, , “जिसे दो अक्तूबर, 2009 में मनरेगा कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से यह योजना काफी सुर्खियों में है, जिसका कारण है केंद्रीय वित्त मंत्रालय की और से किया गया एक नीतिगत परिवर्तन। इससे मनरेगा भी अब अन्य योजनाओं की तरह वित्तीय खर्च सीमा के दायरे में आ गई है। मनरेगा मतलब ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इसे एक मांग आधारित योजना कहा जाता है। मांग अर्थात हर एक वह ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, वे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों तक रोजगार की मांग कर काम पा सकते हैं। मांग का सीधा तात्पर्य है कि जब जरूरत हो, तब रोजगार दिया जाएगा और उसका भुगतान होगा। मांग किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न हो पाने पर मांगकर्ता राज्य सरकारों से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। रोजगार की फिक्र और और खर्च का दायरा
बेरोजगारी भत्ता आरंभिक तीस दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा बाद की अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा। नियमानुसार कार्य में आधी आबादी को वरीयता देते हुए न्यूनतम एक तिहाई महिला लाभार्थी होनी चाहिए। रोजगार पांच किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा। यदि यह पांच किलोमीटर से अधिक है, तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर श्रमिकों के दुर्घटना के शिकार होने पर प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है। इसके अलावा कार्यस्थल पर मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अनुग्रह र राशि भी प्रदान की जाती है। मनरेगा इतनी सारी खूबियों के साथ कुल मिला कर जरूरतमंद को काम देने के निमित्त सरकार को नैतिक रूप बाध्यकारी बनाती है, जो वित्तीय दायरे को पार कर सकती है, इसलिए यह एक योजना के साथ कानून भी है। मगर, अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना को भी मासिक या त्रैमासिक (एमएपी/क्यूएफपी) व्यय से बांधने की ओर कदम बढ़ाया है।
मासिक या त्रैमासिक व्यय केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद सरकारी विभागों का अपने खर्च पर सख्त निगहबानी करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि खर्च बजटीय प्रावधानों के अनुरूप ही चले। मनरेगा को भी अब मासिक या त्रैमासिक व्यय के तहत चलाने के क्रम में पहली बार वित्त वर्ष 2025 2026 की प्रथम छमाही में कुल वार्षिक बजट 6,000 करोड़ रुपए आबंटन के सापेक्ष अधिकतम साठ फीसद यानी 51,600 करोड़ रुपए खर्च की सीमा रेखा तय कर दी गई है है आठ जून, 2025 तक इस योजना के कुल बजट का 28.47 फीसद ही खर्च हो पाया , जबकि वित्तीय वर्ष 2024 2025 का लंबित भुगतान 21,000 करोड़ रुपए है। मासिक या त्रैमासिक व्यय सीमा लागू होने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत में अधिक खर्च की मांग की थी और इस नई व्यवस्था का विरोध किया, मगर वित्त मंत्रालय ने नकदी प्रवाह के बेहतर प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने का तर्क देकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
विलंबित भुगतान के संबंध में यह गौर करने लायक है कि मनरेगा अधिनियम के तहत पंद्रह दिनों के भीतर पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि दैनिक मजदूरी का वितरण किसी भी मामले में उस तारीख से एक पखवाड़े के बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रावधानों के ठीक उलट कई राज्यों में महीनों से मनरेगा
के तहत भुगतान सहित अन्य देनदारियां लंबित पड़ी हैं। इन्हीं सब कारणों से बीते वित्तीय वर्ष 2024 2025 का तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा वर्ष 2006 में जब शुरू की गईं, तो यह पहले चरण में देश के मात्र 200 जनपदों में ही लागू की गई। बाद में वित्तीय वर्ष 2008-2009 में इसकी सफलता को देखते हुए इसे सौ फीसद शहरी क्षेत्रों को छोड़ते हुए पूरे देश में लागू कर दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों से पलायन को कम करना, अकुशल श्रमिकों के रोजगार को सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्रय शक्ति को बढ़ावा देना, गांवों में गरीबी व अमीरी का भेद कम करना, गांवों अस्थायी व स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है।
वित्तीय इन उद्देश्यों में मनरेगा काफी हद तक कामयाब भी रही है, फलस्वरूप वर्ष 2020 2021 -2021 के दौरान कोरोना काल में जब शहरों के बजाय गांवों की तरफ पलायन शुरू हुआ तो मनरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए संकटमोचक बनकर खड़ी हुई। उस समय रेकार्ड 7.55 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 2025 में मात्र 5.79 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला।”
आश्चर्य की बात है कि पर्याप्त बजट और समय से भुगतान का प्रावधान होने के बावजूद ‘दशकों से । यह योजना पूरे देश में चल रही हैं, फिर भी 21,000 करोड़ रुपए की देनदारियां कैसे अटक गईं? वित्त मंत्रालय का तर्क है कि इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए अब सभी योजनाओं की तरह मनरेगा को भी मासिक या त्रैमासिक व्यय के दायरे शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय का मानना है इस कदम से राज्यों पर तय समय सीमा के भीतर भुगतान करने का दबाव बनेगा और देनदारियां कम होंगी, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों और नीति, रीति के जानकारों के बीच बहस का विषय यह कि जब मनरेगा एक मांग आधारित योजना, तो अधिक काम की मांग होने पर तयशुदा बजट कैसे आर्थिक प्रतिपूर्ति कर पाएगा।
संभवतः यह पहली ऐसी योजना है, जो जनकेंद्रित और नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली है। मांग निचले स्तर अर्थात ग्राम पंचायतों से आती है तो इसे साठ फीसद खर्च से क्यों बांधा जाए? पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता है कि मनरेगा को खर्चे में बांध देने से अगर रोजगार की अधिक मांग आ गई तो रोजगार कैसे दिया जाएगा नई व्यवस्था से लंबित बकाया की बड़ी धनराशि पुराने भुगतान में चली नतीजतन नए रोजगार सृजन की संभावनाएं कम हो सकती हैं। ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि आगे की राह सुगम करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों, श्रमिकों व मनरेगा से संबंधित अकुशल समस्त कार्मिकों के भरोसे की बहाली के लिए लंबित देनदारियों के शीघ्र निपटारे की समुचित व्यवस्था की जाए और भविष्य में ऐसे दुरें पर न जाने के लिए कुछ ठोस रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से बेहतर समन्वय स्थापित करे, जिससे कार्य आसान हो, खर्च नियंत्रण जमीनी हकीकत के आधार पर हो व पारदर्शिता और पुख्ता हो । सरकार द्वारा मनरेगा का मूल ढांचा अर्थात मांग आधारित प्रावधान बरकरार रखते हुए खर्चे की सीमा भले ही नियत कर दी गई है, मगर आवश्यकता पड़ने पर तत्काल धनराशि जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद को सही समय पर काम व उसका दाम मिल सके जाएगी। रोजगार की फिक्र और और खर्च का दायरा