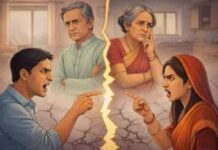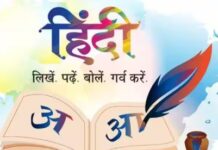मनुष्य का अंतःकरण महत्वपूर्ण है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चेतन और अहंकार 4 घटक हैं। अंतःकरण अनुभव में आता है। उसके प्रपंच शरीर के माध्यम से बाहर प्रकट होते हैं। अंतःकरण विशेष परिस्थितियों में मन कहलाता है। शंकराचार्य के अनुसार, “अंतःकरण की चार आकृतियां होती हैं-संदेह, निश्चय, चेतना और स्मरण। संदेह की स्थिति में इसे मन कहते हैं। निश्चय की स्थिति में इसे बुद्धि कहते हैं। आत्म चैतन्य की स्थिति में इसे अहंकार कहते हैं। एकाग्रता और स्मरण की स्थिति में इसे चित्त कहते हैं।“ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को मन की चंचलता दूर करने और नियंत्रित करने के उपदेश दिए थे। अर्जुन ने प्रतिप्रश्न पूछा था कि, ”मन बड़ा चंचल है। उसे केन्द्रीभूत करना कठिन है-चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्”। मन का निग्रह वायु को पकड़ने जैसा कठिन काम है। शिव संकल्प से भरा हो हमारा मन
शरीर और मन अलग नहीं हैं। शरीर प्रत्यक्ष है, इसी का सूक्ष्म हिस्सा मन है। दोनों एक हैं। साइको सुमेटिक हैं। मन को एक केन्द्र पर लाना भारतीय दार्शनिकों का प्रिय विषय रहा है। ऋग्वेद के ऋषियों ने सीधे मन से ही प्रार्थना की थी, ”हे मन तुम यहां वहां, वन, पर्वत और आकाश तक विचरण करते हो। यहां आओ। यहीं रुको। यहीं तुम्हारा जीवन है।” यजुर्वेद में मन को लोक कल्याण से भरने की स्तुतियां हैं, ”हमारा जो मन यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता है। वह शिव संकल्प से भरा पूरा हो। लगातार 6 मंत्रों के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु की टेक है।” सभी 6 मंत्रों को अलग से शिव संकल्प सूत्र कहा जाता है। सारांश है कि मन की गति असीम है। समय की छोटी इकाई पल होती है। आंख खोलने में जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं। मन पल से भी कम समय में आकाश पहुंचता है। मैं सोचता हूं कि क्या हमारा मन समूचे दिक्काल का भी अतिक्रमण करता है? संसार दिक्काल के भीतर है और मन मनुष्य के भीतर।
मन के अध्ययन की कठिनाई है। यह हमारे शरीर का प्रत्यक्ष अंग नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है। गीता में शरीर के परे मन बताया गया है। मन के परे बुद्धि और बुद्धि के परे आत्मा। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानव दर्शन में व्यक्ति को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा-बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस और सोल कहा है। उन्होंने भूमि और जन को राष्ट्र का शरीर बताया है। इस भूमि के सभी जनों के साथ-साथ रहने की इच्छा भारत का मन है। धर्म राष्ट्र की बुद्धि है और राष्ट्र व विश्व को परिवार जानने की जिजीविषा भारत की आत्मा है। मन का अध्ययन बड़ा प्यारा है। मन का स्वभाव मनमानी है। मन रसिक है। अभिलाषा से भरा पूरा है, इसीलिए वह मर्यादा तोड़कर मनमानी करता है। बुद्धि के पास रस नहीं होता। बुद्धि रूखी होती है। उसे तर्क चाहिए। प्रश्न, तर्क और प्रत्यक्ष बोध उसके उपकरण हैं। रस न हो तो मनुष्य रूखा हो जाता है।
भारतीय दर्शन और साहित्य में रस की व्यापक चर्चा है। रस प्रवाह में ही जीवन की गति है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को रस कहा गया है-रसो वै सः। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया, ”रस महत्वपूर्ण है। रसों में जल मैं हूं।” श्रीकृष्ण संसार की सभी विभूतियों में परम सत्ता की ही उपस्थिति बता रहे थे। रस महत्वपूर्ण है। शरीर की नाड़ियों में रक्त रस का संचार चला करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से रक्त लाल और श्वेत अणुओं का संगम है। श्वेत रक्त कणिकाओं में स्नोफिल, बैसिमर आदि अनेक रक्त घटक भी हैं। मन में आता है कि क्या रक्त के सभी घटक जान लिए गए हैं। अगर जान लिए गए होते तो वैज्ञानिक कृत्रिम रक्त बना सकते थे। कृत्रिम रक्त अभी उपलब्ध नहीं है। रक्त के अध्ययन में कोई घटक पकड़ से बाहर चला गया है। शरीर की आंतरिक गतिविधियों में ही ऐसा कारखाना है जहां रक्त निर्माण होता है। प्रश्न है कि रक्त घटकों में छूट गए अज्ञात अंश को क्या नाम दें? बुद्धि के प्रपंच जान लिए गए हैं। इसीलिए कृत्रिम बुद्धि-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हो गया है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की बुद्धि से ही पैदा हुई। पता नहीं इसे आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं। इसे मनुष्य की ही बुद्धि का एक विकास कहा जाना चाहिए।
मनुष्य शरीर रहस्यपूर्ण है। मनुष्य मस्तिष्क में पूरा ब्रह्माण्ड भरा हुआ है। प्रेम और प्यार मस्तिष्क में हैं। प्रसन्नता और आनंद के केन्द्र मस्तिष्क में है। ईष्र्या, द्वेष और राग मानव बुद्धि का हिस्सा हैं, लेकिन इस सबके लिए प्रसन्न मन के साथ स्वस्थ शरीर भी आवश्यक है। अपने मन को सब लोग निर्णायक और सही मानते हैं। कहते हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। ऐसा करते भी हैं। शरीर भी अपनी सुनाता है। हम शरीर की नहीं सुनते। हम पान मसाला और तंबाकू खाते हैं। शरीर विद्रोह करता है। शरीर के विद्रोह से ही थूक निकलता है। शरीर इनकार करता है कि उसे यह स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हम शरीर की नहीं सुनते। शरीर अपने लिए उपयोगी और नुकसानदेह का निवारण खुद तैयार करता है। किसी कारणवश मुंह में छोटा सा कीड़ा या भुनगा चला जाता है, शरीर विद्रोह करता है। शराब और दारू भी शरीर स्वीकार नहीं करता। लती पियक्कड़ भी पहले घूंट से ही मुंह टेढ़ा करने लगते हैं। हम शरीर की बात नहीं सुनते। अपने मन की करते हैं।
मन यूरोपीय विद्वानों के लिए भी गहन अध्ययन का विषय रहा है। दुनिया के मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी सिगमंड फ्रायड ने मन का गहन विश्लेषण किया था। ’साइको एनालिसिस’ उसकी महत्वपूर्ण किताब है। सपनों पर उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ-’दि इंटरप्रेटेशन ऑफ ड्रीम्स’ है। यह विश्लेषण भी बड़ा प्यारा है। उसने मन के कई तलों की व्याख्या की है। लिखा है कि रोगों का सम्बंध भी मनोविकारों से है और सपनों से भी। प्रतिभा और प्रतिष्ठा को भी फ्रायड ने मन की लिविडो की ही करामात बताया है। फ्रायड (1856-1939) अभी-अभी 19वीं व 20वीं सदी में हुए हैं। अथर्ववेद उससे पुराना है। अथर्ववेद में काव्य सृजन और स्वप्नों को काम भावना से जोड़ा गया है। ऋषि कहते हैं कि, ”हे काम, कविता तुम्हारी पुत्री है और तुम हमारे पास स्वप्न भी भेजते हो। दुःस्वप्न न भेजा करो।“ पतंजलि का मनोविश्लेषण ज्यादा वैज्ञानिक है। योगसूत्र पतंजलि की लिखी ऐतिहासिक पुस्तक है। इसकी शुरुआत का श्लोक दो शब्दों का है-’अथ योगानुशासन’-अब हम योग के अनुशासन में जाते हैं। योग की परिभाषा करते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः-चित्त की वृत्तियों को समाप्त करना योग है। तुलसीदास भी मनोविकारों के प्रभाव से परिचित थे। रामचरितमानस में लिखा था, ”काम वात कफ लोभ अपारा/क्रोध पित्त नित छाती जारा अर्थात काम भावना से वायु, लोभ से खांसी, क्रोध से पित्त खराब होता है। सीने में जलन होने लगती है। आगे कहते हैं, ”प्रीति करहि जो तीनों भाई/उपजहि सन्निपात दुखदायी। काम, क्रोध व लोभ तीनों मनोविकारों के एक साथ होने से सन्निपात हो जाता है। हम शरीर की सुनें। मन की सुना ही करते हैं। बुद्धि की सुनें। पिता, माता और आचार्य की सुनें। सबको सुनें। मनमानी न करें।” तन्मे मनः शिवसंकल्पम् अस्तु। शिव संकल्प से भरा हो हमारा मन