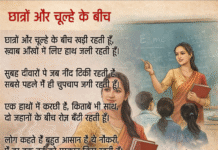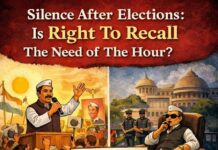हम असीम अस्तित्व के अंग हैं। इसलिए लघु से महत होने की संभावनाएं भी हैं। हम शरीरधारी हैं। हमारी पहली सीमा शरीर है। इससे सम्बंधित बड़ी सीमा परिवार है। परिवार के बाद बड़ी संस्था है समाज। परिवार तक ही सीमित रहे तो समाज से अलग रहते हैं। यूरोप और अमेरिकी समाज परिवार से भी पहले वाली सीमा में है। वे व्यक्तिवादी हैं। भारत में परिवार और समाज से राष्ट्रभाव का विकास हुआ है। भारतीय पूर्वज राष्ट्र की सीमा के बाहर भी आत्मीय रूप में संवेदनशील थे। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की अनुभूति भारतीय चिन्तन से ही निकली है। इसके बाद आकाश, सौरमण्डल और फिर असीम ब्रह्म विस्तार का आच्छादन। यहां इकाई अनंत हो गई है। मैं इन पंक्तियों का लेखक भारतीय समाज की जाति सच्चाई के अनुसार ब्राह्मण जाति का हूं। जाति सीमा को तोड़कर बाहर आऊं तो मानव समाज का हिस्सा हूं। हम इसे और गहरे अनुभव करते हैं तो मैं विश्व मानवता का सदस्य। इसे और फैलाता हूं तो प्रकृति का भाग हूं। अब मैं कीट, पतिंग और वनस्पति जगत का भी सहोदर हूं। मैं अन्ततः ब्रह्माण्ड का हिस्सा हूं। आखिरकार हम हैं कौन..?
संपूर्णता पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण घटाओ तो पूर्ण ही बचता है। सम्पूर्णता आनंदित करती है। संसार का ज्ञान जरूरी है लेकिन हम स्वयं से पूरा परिचित नहीं हैं। आखिरकार हम हैं कौन? प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। हम ही प्रश्नकर्ता है और हम उत्तरदाता। मोटे तौर पर हम सबका उत्तर होगा कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ है मनु के। मनु का उल्लेख ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में भी है। दर्शन अनुभूति में हम चेतन हैं। लोकव्यवहार में हम भारतीय अमेरिकी या जापानी वगैरह भी है। हम विराट प्रकृति का अंग है। आस्तिकता के कारण हम जरथुस्त्र, ईशा, इस्लाम या भारतीय धर्म के अंग हैं। हमारे बहिरंग परिचय के अनेक रूप हैं। हम पिता हैं, पुत्र हैं। अनेक रिश्तों के बंधन में हैं। अनेक परिचय हैं हमारे। हम किसी न किसी जाति के भी हैं और जाति में होने का कारण हमारा किसी समूह विशेष में जन्म लेना ही है।
लेकिन भारत में जातियां सामाजिक यथार्थ हैं। वे न होतीं तो अच्छा होता। जातियां सामाजिक एकता में बाधक हैं। जाति सामाजिक सच्चाई है। जातियां जन्मना हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी जाति नहीं चुन सकता। इनका ढांचा सोपान क्रम में है। इसके शीर्ष वाली जातियों का सम्मान रहा है। सीढ़ी में निचली जातियां काफी लम्बे समय से सामाजिक सम्मान से भी वंचित रही हैं। डाॅ0 अम्बेडकर ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय (1916) में “जातियों की उत्पत्ति और संरचना” पर शोध प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था “प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न वर्ग होते हैं। बौद्धिक आर्थिक या अन्य कारणों से बने वर्ग अपना अस्तित्व भी रखते हैं। भारत में भी ऐसे ही वर्ग रहे होंगे। पुरानी भारतीय वर्ण व्यवस्था को कर्मश्रम आधारित वर्ग कहा जा सकता है। पहले वर्ण जन्मना नहीं थे। वर्ग भी जन्मना नहीं होते। डाॅ0 अम्बेडकर ने कहा कि, “किसी समय किसी एक वर्ग वर्ण ने अपने ही वर्ण वर्ग में विवाह करने का बंधन लगाया होगा।” वे कहते हैं “जाति के उद्भव के अध्ययन से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि वह वर्ग कौन सा था जिसने अपने लिए बाड़ा खड़ा किया। मैं इसका प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। हिन्दू समाज में कुछ प्रथाएं सर्वव्यापी थीं। अपने समस्त प्रतिबंधों के साथ वे ब्राह्मणों में थीं। ब्राह्मण वर्ग ने स्वयं की घेराबंदी जाति रूप में क्यों की? यह एक भिन्न प्रश्न है?” प्रश्न उचित है। ऋग्वैदिक काल में जाति वर्ण नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण हैं। वर्ण जन्मना नहीं थे। इसलिए जाति नहीं थी। जाति की जन्मतिथि खोजना असंभव है। जाति बंधन मजबूत है।
ब्राह्मणों पर जाति प्रथा लागू करने के आरोप अक्सर लगाए जाते हैं। डाॅ0 अम्बेडकर ने इसी शोध में कहा था, “जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास एक विशाल कार्य था। ब्राह्मण अनेक गल्तियां करने के दोषी रहे हों, कह सकता हूं कि वे ऐसे थे लेकिन जाति व्यवस्था को गैर ब्राह्मणों पर लाद सकने की क्षमता उनमें नहीं थी।” सही बात है। कोई शक्तिशाली राजव्यवस्था भी अपने शासित लोगों के बड़े वर्ग समूह को जन्मना किसी जाति में ही रहने के लिए विवश नहीं कर सकती। जाति का उद्भव पूर्वजों के अचेत कर्म का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन की निरंतरता में जन्मना जातियां बनी। लेकिन हमारे सचेत पूर्वजों ने जाति समाप्ति के लिए अथक श्रम भी किये। गांधी, डाॅ0 अम्बेडकर, डाॅ0 हेडगेवार, डाॅ0 लोहिया, ज्योतिबा फुले और विवेकानंद दयानंद ने भी जाति भेद के विरोध में नवजागरण किया। इस श्रम के बावजूद कतिपय लोगों ने दलित जातियों को जब कब भिन्न नस्ल भी बताया। डरबन में अगस्त 2001 में “नस्लवाद, नस्ली भेदभाव और असहिष्णुता” पर विश्व कांग्रेस का आयोजन था। भारत के कुछेक लोगों ने उस वक्त दलितों को अलग नस्ल बताया था लेकिन डाॅ0 अम्बेडकर ने दलितों को कभी भी अलग नस्ल नहीं माना था। उन्हें उम्मीद थी कि जातियां खत्म ही होंगी। लिखा था “जाति का चलते रहना असंभव है। ऐसा कार्य दिक्कतों से भरा है।” सामाजिक समता अनिवार्य है। सामाजिक न्याय की दिशा में बेशक भारत का काम आगे बढ़ा है। जाति की अस्मिता ज्यादा दिन नहीं चल सकती है।
राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का काम भी करना चाहिए। जाति की विभाजनकारी शक्ति के विरूद्ध जनअभियान चाहिए। संविधान निर्माताओं ने जाति, लिंग या धर्म के आधार पर विभेद का निषेध किया है बावजूद इसके उत्पीड़न या प्रतिष्ठा जैसे सभी अवसरों पर जाति की पहचान आगे चलती है। अपने जिले या राज्य क्षेत्र में किसी के भी प्रतिष्ठित होते ही जाति के प्रश्न उठ जाते हैं। अनुसूचित या अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिष्ठित होने वाले लोग आशावाद भी जगाते हैं। वे वंचित निराश लोगों की प्रेरणा भी बनते हैं। दलित या अन्य पिछड़ा वर्ग होने के बावजूद कोई प्रतिष्ठा का आकाश छू रहा है तो उसी वर्ग के सामान्यजन भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
जाति का कोई औचित्य नहीं है। भारत को जातिभेदविहीन समाज बनाना होगा। “सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय” भारतीय संविधान की उद्देशिका के मूल तत्व है। राजनैतिक न्याय ने मताधिकार दिया है। सरकारें विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। प्रशासन उत्तरदायी नहीं है। वंचित वर्गो के लिए बहुत सारा नीति निर्माण हुआ है तो भी प्रशासनिक संवेदनहीनता के चलते सामाजिक न्याय दूर है। दार्शनिक क्षेत्र में भारत विश्वप्रतिष्ठ है। यहां कण-कण में परमात्मा की बाते कही जाती हैं लेकिन जन जन में जाति है और जाति भेद भी है। जाति की चर्चा से बचा नहीं जा सकता। सामाजिक यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। एकात्मवादी विचार आदर्श है। इस विचार के लिए विमर्श भी जरूरी है। परंपरा के साथ विज्ञान और जाति मुक्त चिन्ता के साथ जाति समूहों का व्यथा चिन्तन भी होना चाहिए। जाति अतिक्रमण का यही मार्ग है। यह काम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और धर्मगुरूओं को भी करना चाहिए। आखिरकार हम हैं कौन..?