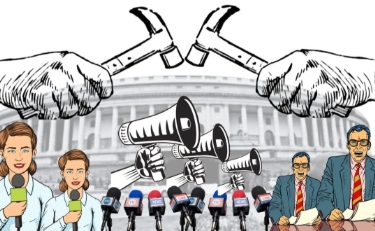

—– 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस —–
“लोकतंत्र की रीढ़ या बाज़ार का शोर? प्रेस की स्वतंत्रता की परीक्षा।” प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। जब पत्रकार निर्भय होते हैं, तब नागरिक सुरक्षित होते हैं।लेकिन आज सत्ता, बाज़ार और डिजिटल शोर के बीच सत्य की आवाज़ दबती जा रही है। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और ट्रेंडिंग कंटेंट ने पत्रकारिता की गंभीरता को चुनौती दी है। राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि यदि सवाल पूछने का साहस खत्म हो गया, तो लोकतंत्र भी केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता ही राष्ट्र की चेतना और जनमत की असली रक्षा करती है। प्रेस की स्वतंत्रता की परीक्षा
भारत हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है—एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की मज़बूती का असली आधार सत्ता नहीं, सत्य की निर्भय अभिव्यक्ति है। यह दिन केवल पत्रकारों का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के विवेक का पर्व है। क्योंकि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसके नागरिकों को सच्चाई तक पहुँचने का अधिकार मिले और उसके पत्रकारों को सत्य कहने का साहस।
प्रेस की स्वतंत्रता दरअसल शब्दों की नहीं, विचारों की स्वतंत्रता है। यह केवल घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व नहीं, बल्कि उन सच्चाइयों को उजागर करने का संकल्प है जिन्हें सत्ता, व्यवस्था या समाज अक्सर छिपा देना चाहता है। पत्रकारिता की यही निडरता लोकतंत्र को जीवंत रखती है—क्योंकि सत्ता को नियंत्रित करने का सबसे मजबूत माध्यम न बंदूक है, न क़ानून, बल्कि क़लम की नैतिकता है।
1975 के आपातकाल के दौरान जब सेंसरशिप ने प्रेस का गला घोंट दिया था, तब भारतीय लोकतंत्र ने अपनी सबसे कड़ी परीक्षा दी। कई अख़बारों ने डरकर खाली कॉलम छापे, कई पत्रकारों ने जेलें देखीं, और कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। यही कारण है कि यह दिवस उन संघर्षों का स्मरण भी है, जिन्होंने साबित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता कोई कृपा नहीं—यह लोकतंत्र का जन्मसिद्ध अधिकार है।
आज डिजिटल युग ने पत्रकारिता को नई गति दी है, पर उसी के साथ अभूतपूर्व चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। खबरों की यात्रा अख़बारों से मोबाइल स्क्रीन तक आ गई है। परंतु हर तेज़ समाचार विश्वसनीय हो, यह ज़रूरी नहीं। एल्गोरिद्म तय करते हैं कि जनता क्या देखेगी, और व्यूज़ यह तय करते हैं कि क्या “खबर” कहलाएगा। यही वह बिंदु है जहाँ पत्रकारिता और मनोरंजन की रेखाएँ धुंधली पड़ गई हैं।ऐसे समय में प्रेस की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है—क्योंकि जब सूचना का प्रवाह अनियंत्रित हो, तब सत्य की स्पष्टता ही एकमात्र मार्गदर्शक बनी रह जाती है।
पत्रकारिता का मूल यह नहीं है कि कौन सबसे पहले खबर दिखाता है; बल्कि यह है कि कौन सबसे पहले साहसपूर्वक सत्य दिखाता है। भारत के असंख्य पत्रकार आज भी गाँवों की कच्ची पगडंडियों से लेकर महानगरों की चकाचौंध तक, अपराध, भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय को उजागर करने में लगे हैं। वे अक्सर बिना सुरक्षा, बिना संसाधन और बिना संस्थागत संरक्षण के काम करते हैं। सच कहें तो पत्रकारिता आज भी एक पेशा नहीं—एक जोखिमभरा संघर्ष है।
प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है। फेक न्यूज़, आधा–सच और सनसनीखेज़ रिपोर्टिंग ने समाज में भ्रम फैलाया है। इसलिए पत्रकारिता की नैतिकता उसके अस्तित्व की पहली शर्त है। एक स्वतंत्र प्रेस तभी सम्मान पाती है जब वह निष्पक्ष, तथ्याधारित और जनहित में काम करे। सत्य को तोड़ने–मरोड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं, अराजकता है।
सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता को सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्फ्लुएंसर और पत्रकार के बीच की दूरी कम होती जा रही है। जहाँ पत्रकार सत्य का पीछा करता है, वहीं इन्फ्लुएंसर ट्रेंड का। पत्रकार का लक्ष्य तथ्य होता है, इन्फ्लुएंसर का लक्ष्य व्यूज़। दुखद यह है कि कई बार जनता भी सरल मनोरंजन को कठिन सत्य पर प्राथमिकता देने लगी है। यदि समाज सच सुनने की इच्छा खो देगा, तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी धीरे-धीरे महत्वहीन हो जाएगी।
स्वतंत्र प्रेस केवल पत्रकारों की लड़ाई नहीं—यह नागरिकों का अधिकार है। नागरिक जितने जागरूक होंगे, प्रेस उतना ही निर्भीक होगा। अगर जनता आलोचनात्मक सोच खो देगी, तो प्रेस केवल बाज़ार और सत्ता का उपकरण बनकर रह जाएगी। इसलिए लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक अपने समाचार स्रोतों से क्या अपेक्षा रखते हैं—सच? या मनोरंजन?
यह चुनाव आने वाले समय में पत्रकारिता की दिशा तय करेगा।आज भारत का मीडिया अनेक दबावों के बीच काम करता है—राजनीतिक, आर्थिक, कॉर्पोरेट और सामाजिक। कई बार सच्चाई कहने का परिणाम नौकरी जाना, मुकदमों में फँसना या जान जोखिम में डालना होता है। इसके बावजूद सैकड़ों पत्रकार आज भी निडर होकर लिखते हैं, बोलते हैं और मैदान में उतरते हैं। उनका साहस हमें यह याद दिलाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कागज़ पर नहीं, जमीनी संघर्षों से जीवित रहती है।
राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह चेतावनी देना भी है कि प्रेस कमजोर हुआ तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। जब सवाल पूछना अपराध बन जाए और चुप्पी सुरक्षा का साधन, तब लोकतंत्र का हृदय मंथर होने लगता है। इसीलिए पत्रकारिता को पुनः उस मूल स्थान पर लौटना होगा जहाँ सच्चाई सर्वोच्च हो—न मालिक से डर, न बाज़ार से, न व्यवस्था से।
समाज के लेखकों, कवियों, शिक्षकों और विद्वानों पर भी यह जवाबदेही है कि वे पत्रकारिता की इस गिरावट और दबाव को समझें। एक राष्ट्र केवल विज्ञान, उद्योग या सेना से महान नहीं बनता; वह महान तब बनता है जब उसमें विचार, संवाद और सत्य की संस्कृति जीवित हो। और यह संस्कृति प्रेस के बिना संभव नहीं है।
अंततः यह समझना आवश्यक है कि प्रेस की स्वतंत्रता सिर्फ एक संवैधानिक प्रावधान नहीं—यह राष्ट्र की नैतिक आत्मा है। जहाँ प्रेस डरकर लिखे, वहाँ समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जहाँ पत्रकारिता सवाल पूछने से हिचक जाए, वहाँ लोकतंत्र धीरे-धीरे रस्म में बदल जाता है। 16 नवंबर इसीलिए महत्वपूर्ण है—क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि एक राष्ट्र उतना ही स्वतंत्र है,जितना उसका पत्रकार स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता की परीक्षा
























