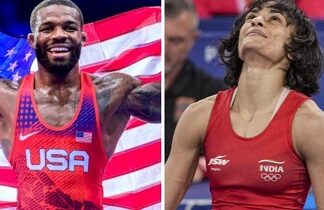जीवन प्रकृति का उपहार है। कोई जन्म लेता है। जन्मा शिशु हंसता है। हाथ पैर चलाता है। परिवार छोटे बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। फिर आती है जीवन की चुनौतियां। दुख आते हैं। सुख आते हैं। वे बारी-बारी से आते जाते हैं। परिवार बढ़ता है। वह वृहत्तर समाज का अंग हो जाता है। वह जैसा चाहता है, वैसा नहीं होता, तो उसे दुख होता है। दुख और सुख आते जाते हैं। दुख स्वयं निरपेक्ष नहीं है। दुख सुख का अभाव है। दुख का मुख्य कारण आसक्ति है। माना जाता है, माया मोह में फंसकर व्यक्ति दुखी रहता है। बुद्ध ने दुख को ही समस्या का जड़ माना है। प्रकृति का उपहार है जीवन
शब्द ’माया’ लोक जीवन में बहुत चलता है। संसार के प्रति आसक्ति के लिए भी ’माया’ शब्द का प्रयोग होता है। तब उसे माया मोह कहते हैं। संसार को कागज की पुड़िया बताने वाले संत कबीर भी माया को ठगनी बताते हैं। एक पूरी सभ्यता को ही ’माया सभ्यता’ कहा जाता है। माया सभ्यता मध्य अमेरिका के दक्षिणी मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला बेलीज पश्चिमी होंडुरस और एल साल्वाडोर तक फैली हुई थी ऋग्वेद में एक शब्द आया है ’ऋभु’। ऋभु कारीगर हैं। एक मंत्र के अनुवाद में ऋभुओं द्वारा बहुत सुंदर स्थापत्य बनाने की प्रशंसा की गई है। माया किसी ने किसी रूप में भारत के मन में बहुत गहराई से बैठी हुई प्रतीत होती है। तुलसीदास भी सांसारिक दुखों का कारण माया बताते हैं। माया प्रभावित जीव दुखी रहते हैं।
माया संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है जो नहीं है, अर्थात हमारे इन्द्रियबोध को धोखा देने वाला। अद्वैत दर्शन में माया की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सत्य सुव्यवस्थित है कि परमार्थतः ब्रह्म ही एकमात्र सत् है। ब्रह्म एक निर्गुण निर्विकार भेदरहित सत्ता है। ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। बाकी सब मिथ्या है। लेकिन सांसारिक जीवन में कुछ जिज्ञासाएं भी चला करती हैं। ब्रह्म की सत्ता पर पूर्ण विश्वास न करने वाले विद्वान कहते हैं कि सांसारिक जीव ऐसा अनुभव नहीं करते। उनके अनुसार जगत् में उन्हें जगत् जीव प्रपंच के अनुभव दिखाई पड़ते हैं। वैसे भी विद्वतजनों में मतभेद बने रहना स्वाभाविक है। मूलभूत प्रश्न है कि इस संसार के सारे प्रपंच और ब्रह्म से उनके सम्बंध क्या हैं?
संसार में जैव विविधता है। मत भिन्नता भी है। जीवन के बारे में अनेक दृष्टिकोण हैं। कुछ मानते हैं कि यह जीवन और जगत् किसी सर्वशक्तिशाली परम शक्ति के द्वारा दिया गया है। उसे ईश्वर की संज्ञा दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे चिंतक विचारक भी हैं, जो जीवन जगत् के लिए प्रकृति की शक्तियों पर निर्भर हैं। अद्वैत वेदांत में केवल ब्रह्म को ही माना गया है। उनका ब्रह्म संसार नहीं बनाता। शंकराचार्य ने ब्रह्म को मात्र एक पारमार्थिक सत्ता बताया है। फिर प्रत्यक्ष संसार की गतिविधियों का रहस्य क्या है? प्रत्यक्ष भौतिक जगत् को माया रूप देखना तथ्यगत नहीं जान पड़ता। शंकराचार्य के अनुसार माया भावात्मक है। अविद्या अभावात्मक है। सुर नर मुनि भी माया के पाश में बंधे रहते हैं। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म ईश्वर है, किंतु विद्या में प्रतिबिंब ब्रह्म जीव है। माया ईश्वर को भी प्रभावित करती है, जबकि अविद्या जीव को प्रभावित करती है। अविद्या त्रिगुणात्मक है। अज्ञान, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, भ्रांति आदि शब्द एक जैसे हैं। इस तरह माया जड़ है और अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है।
उपनिषदों में विद्या और अविद्या शब्द आए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आसक्ति के कारण यह संसार खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दुख आने पर यह संसार वैसा नहीं दिखाई पड़ता जैसा हम सोचते हैं। दर्शन में ऐसे प्रश्नों पर गंभीर विचार हुआ है। प्रश्न है कि, यह विश्व किस तरह अस्तित्व में आया? क्या इसे किसी ने बनाया है? क्या यह सदा से है? अगर किसी देव शक्ति ने बनाया है, तो इस रचना के पहले कुछ तो रहा ही होगा? कोई वस्तु पदार्थ अथवा अणु परमाणु शून्य से नहीं पैदा हो सकते। वैदिक काल से लेकर उपनिषद काल तक यह धारणा रही है कि ईश्वर शासक नहीं है। वह करुणानिधान है। वह सर्वशक्तिमान सत्ता है। जो समस्या भारत में ऋषियों के सामने थी, वही समस्या यूनानी दार्शनिकों के मध्य विचारणीय थी। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि माया और अविद्या में कोई भेद नहीं है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन के द्वैतवाद का खंडन किया है और सांख्य के पुरुष तत्व को ब्रह्म या आत्मा का आसन दिया। माया अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है। माया की शुरुआत कब हुई पता नहीं। अनादि और अनंत में फर्क होते हैं। अनादि वह तत्व है जो सदा से है और अनंत का अर्थ, जिसका अंतिम छोर पता नहीं। शंकराचार्य के अनुसार माया ज्ञान के सामने नहीं बचती। अनादि होकर भी अनंत न होना स्वाभाविक है। वस्तुतः माया ज्ञान प्रकाश मिलते ही समाप्त हो जाती है।
माया अजर अमर नहीं है। वह ज्ञान से बाधित है। माया ज्ञान के समक्ष नहीं बच पाती। यह अभावात्मक भी नहीं है। यदि यह केवल अभाव रूप होती तो इससे सृष्टि का उद्भव असंभव होता। संसार भ्रम से भरा पूरा है। इस तरह माया सत् नहीं है। ब्रह्म से स्वतंत्र उसकी कोई सत्ता नहीं है। माया को सत् या असत् नहीं कहा जा सकता। माया सत् नहीं है। यह यथार्थ ज्ञान से तिरोहित हो जाती है। माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह असत् भी नहीं है। वह जगत् को आरोपित करती है। इसी तरह का माया जैसा एक आंतरिक अनुभव अध्यास है, जो वस्तु नहीं है। उसका अनुभव करना अध्यास है। माया भी ऐसी है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझने तक सत्य का पता नहीं चलता। वहां सांप वास्तव में नहीं होता, लेकिन अध्यास के कारण वह प्रभावी रहता है। माया का आश्रय ब्रह्म है। माया ब्रह्म में रहती है और संसार के आविर्भाव के लिए ब्रह्म को ही अपना विषय बनाती है। अपने सारे काम करते हुए वह प्रभावित नहीं होती। ब्रह्म भी प्रभावित नहीं होता। माया और अध्यास एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, मगर हैं नहीं। माया संसार रचती है। अध्यास के तीन घटक बताए गए हैं। अधिष्ठान, अध्यस्त, अध्यस्त वस्तु और आरोप। यहां अधिष्ठान वह तत्व है जो अध्यास काल में उपस्थित है।
शंकराचार्य के अनुसार अध्यास का कारण अविद्या है। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं होता। विद्या और अविद्या शब्द उपनिषदों से आए हैं। अविद्या का अर्थ है प्रत्यक्ष संसार की वस्तुओं और आचार विचार की सारी कार्यवाहियों का ज्ञान और विद्या का मतलब है परम तत्व का ज्ञान। ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र में कहते हैं कि जो विद्या के उपासक हैं, वे अंधलोकों में जाएंगे और जो विद्या के उपासक हैं। वे भी अंधलोकों में जाएंगे। सांसारिक ज्ञान अविद्या है। अविद्या और विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है। साधक दोनों की जानकारी के लिए उपासना करें। अविद्या से जुड़े होने के कारण अध्यस्त के गुण दोष का कोई प्रभाव अधिष्ठान पर नहीं पड़ता। पुराना उदाहरण लें, जब कोई व्यक्ति अविद्या के कारण रस्सी में सर्प का ज्ञान प्राप्त करता है, तब सर्पत्व का कोई प्रभाव रस्सी पर नहीं पड़ता। अध्यास के प्रभाव में रस्सी सांप नहीं बन जाती। वह सांप जैसी प्रतीत होती है। इससे सर्प ज्ञान बाधित होता है। शंकर के अनुसार अध्यस्त वस्तु अपने मूल रूप में बनी रहती है। इसे असत नहीं कहेंगे। भ्रम काल में भी उसका अनुभव होता है और यह वस्तुतः सही नहीं होता है। हम भारतवासी अध्यात्मबोध को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ऐसा बोध माया की सीमा तक जाता है। माया की सीमा है। वह अनंत नहीं है।